यूएनएचआरसी: आपातकाल के बाद आज भी नागरिक अधिकार संकट

ऐतिहासिक फैसला: जब अदालत ने झुकाया सिर
यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की हालिया समीक्षा भारत की नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाती है। इसकी जड़ें आपातकाल के दौरान सुनाए गए एक ऐतिहासिक फैसले में हैं। 28 अप्रैल 1976 को सर्वोच्च न्यायालय ने ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। बहुमत ने माना कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यहाँ तक कि जीवन के अधिकार को भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की साहसी असहमति भी इस फैसले को रोक न सकी। उस समय तिहाड़ जेल में बंद विपक्षी नेताओं तक यह खबर कई दिन बाद पहुँची। यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया, जिसकी छाया आज भी दिखाई देती है।
वर्तमान परिदृश्य: सुधार का भ्रम
यूएनएचआरसी रिपोर्ट के अनुसार पाँच दशक बीत जाने के बाद भी स्थिति में कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ है। आज का निगरानी तंत्र 1976 की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत और व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर जरूर ऐतिहासिक फैसला दिया, पर व्यवहार में इसका प्रभाव नगण्य रहा है।
कई मामलों में उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों ने नागरिक अधिकारों की रक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। इन अदालतों का प्रक्रियात्मक कानून से सीधा सामना होने के कारण यह संभव हो पाया। फिर भी, कार्यपालिका की शक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं।
कार्यपालिका का बढ़ता दखल: नए रूप में पुरानी समस्या
राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के नाम पर कार्यपालिका ने अपने अधिकारों का दायरा लगातार विस्तारित किया है। नागरिकों में यह भ्रम व्याप्त है कि मतदान करना ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए पर्याप्त है। यह धारणा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।
लोकतांत्रिक चेतना पहले व्यक्ति के मन में मरती है, फिर धीरे-धीरे पूरे समाज में फैल जाती है। आपातकाल के दौरान दिखाई गई न्यायपालिका की निष्क्रियता ने इस प्रक्रिया को गति दी, जिसके परिणाम आज भी दिखाई देते हैं।
आपातकाल की विषाक्त विरासत
यूएनएचआरसी की चिंताओं को समझने के लिए आपातकाल के दीर्घकालिक प्रभावों को समझना आवश्यक है। उस दौर की सबसे खतरनाक विरासत थी न्यायपालिका की स्वायत्तता पर प्रहार। सरकार ने असहमत न्यायाधीशों को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का बार-बार स्थानांतरण किया। जो न्यायाधीश सत्ता के रुख से सहमत नहीं थे, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति नहीं मिली।
आज भी न्यायपालिका में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व नगण्य है, जो समावेशी न्याय प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती है।
निवारक निरोध: सत्ता का हथियार
आपातकाल की सबसे कुख्यात विरासत है निवारक निरोध कानूनों का दुरुपयोग। यूएनएचआरसी रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और राज्य सरकारें आज भी इन कानूनों का खुलकर दुरुपयोग कर रही हैं। 1981 के ए.के. रॉय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को बरकरार रखा, भले ही उसने 44वें संविधान संशोधन को लागू न करने को अनुचित बताया।
इस फैसले ने सरकारों को निवारक निरोध के व्यापक इस्तेमाल की खुली छूट दे दी। परिणामस्वरूप, हिरासत में लेने, रिहाई के आदेशों की अवहेलना और राजनीतिक विरोधियों को लक्षित करने की घटनाएँ आम हो गई हैं।
यूएनएचआरसी की प्रमुख आपत्तियाँ
पिछले वर्ष जुलाई में जारी अपनी रिपोर्ट में यूएनएचआरसी ने भारत में आईसीसीपीआर (ICCPR) के कार्यान्वयन पर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं। समिति ने नोट किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आईसीसीपीआर के प्रावधानों को केवल तभी लागू करता है जब वे घरेलू कानून के अनुरूप हों।
विशेष रूप से अनुच्छेद 9 (स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार) के संबंध में यह स्पष्ट देखा गया कि इसे संविधान के अनुच्छेद 22 तक ही सीमित रखा गया। समिति ने मणिपुर, असम और जम्मू-कश्मीर जैसे “अशांत क्षेत्रों” में आतंकवाद विरोधी कानूनों के दशकों से चल रहे इस्तेमाल पर भी गहरी चिंता जताई।
विशेष कानूनों का दमनकारी इस्तेमाल
यूएनएचआरसी ने स्पष्ट किया कि आईसीसीपीआर के तहत ऐसे विशेष कानून केवल आधिकारिक आपातकाल की घोषणा के बाद ही लागू किए जा सकते हैं। भारत ने किसी भी क्षेत्र के लिए ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों से मानवाधिकार उल्लंघन की निरंतर रिपोर्टें मिल रही हैं, जिनमें अत्यधिक बल प्रयोग, गैरकानूनी हत्याएँ, मनमानी हिरासत, यातना और यौन हिंसा शामिल हैं।
मणिपुर का उदाहरण विशेष रूप से चिंताजनक है जहाँ 1979 से 2012 के बीच 1,528 प्रलेखित न्यायिक हत्याओं में से केवल 39 मामलों में ही एफआईआर दर्ज की गई। अधिकांश मामलों में सरकार ने अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
जेल सुधार और विचाराधीन कैदियों का संकट
यूएनएचआरसी रिपोर्ट ने भारतीय जेलों की दयनीय स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। 2022 के आँकड़ों के अनुसार जेलों में बंद 75% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें मुस्लिम, दलित, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की संख्या अत्यधिक है। समिति ने मनमानी गिरफ्तारी के खतरे और जमानत प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर विशेष चिंता व्यक्त की।
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे कानूनों के तहत तो जमानत मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि इनमें निर्दोषता के सिद्धांत को ही उलट दिया गया है। साथ ही, भारत के नए आपराधिक कानूनों में यातना को स्पष्ट रूप से अपराध न मानना और यातना विरोधी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन की पुष्टि न करना भी गंभीर चिंता का विषय है।
क्या अंतर है? मौलिक प्रश्न
यूएनएचआरसी की 17-पृष्ठीय रिपोर्ट आपातकाल के पाँच दशक बाद भारत की नागरिक स्वतंत्रता की वास्तविक तस्वीर पेश करती है। यह स्पष्ट करती है कि सर्वोच्च न्यायालय आईसीसीपीआर को केवल तभी लागू करता है जब वह घरेलू कानून के अनुकूल हो। इससे एक गंभीर प्रश्न उठता है: क्या संविधान को निलंबित करने वाले आपातकालीन शासन और वर्तमान “सामान्य” शासन में कोई वास्तविक अंतर है?
क्या एक ऐसा तंत्र जो संविधान की मूल भावना को कुचलता है, वह लोकतंत्र कहलाने का अधिकारी है? यूएनएचआरसी की रिपोर्ट इस प्रश्न पर विचार करने की माँग करती है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है – यह प्रत्येक नागरिक की सामूहिक चेतना और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक आपातकाल की विषाक्त विरासत हमारे लोकतंत्र को खोखला करती रहेगी।

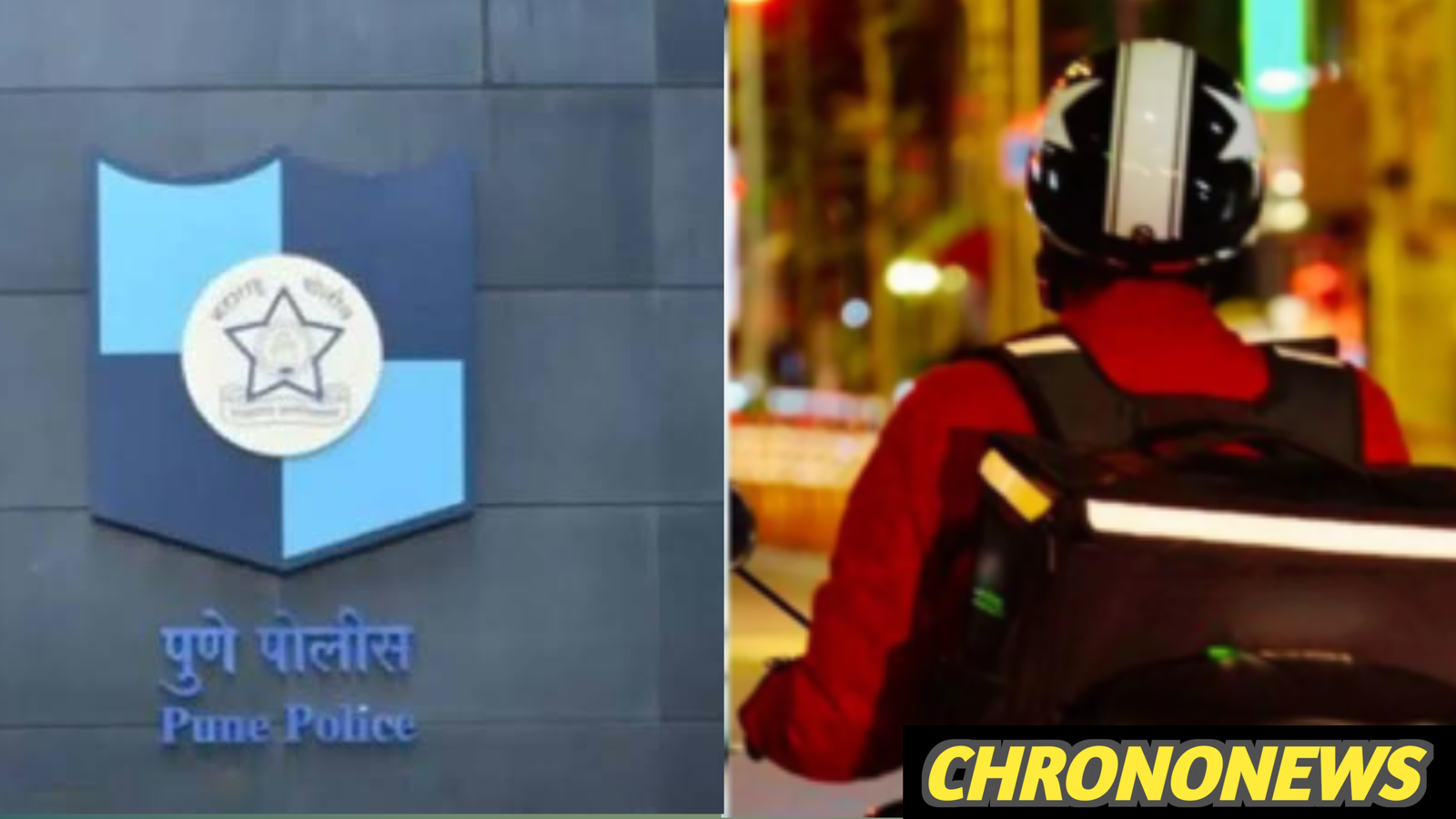

Post Comment